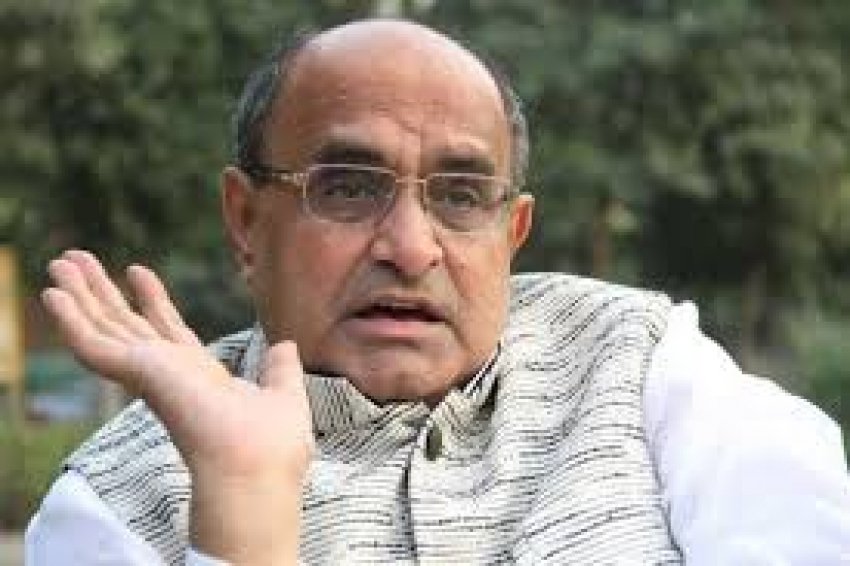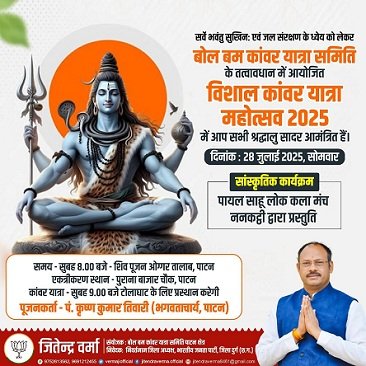शौर्यपथ / कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन से किसानों को हुई क्षति की भरपाई के लिए सरकार काफी सक्रिय है। किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिले और वे अपनी उपज कहीं भी बेच सकें, इसके लिए कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में संशोधन की घोषणा की जा चुकी है। अब तक किसान राज्यों द्वारा अधिसूचित मंडियों में ही उपज बेच सकते हैं, नए कानून के बाद वे इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सरकार ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ में संशोधन करके उपज की स्टॉक सीमा भी खत्म करने जा रही है। इन दोनों कानूनों का मकसद है- संकट की इस घड़ी में किसानों के हितों की रक्षा करना। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में कृषि और किसानों के लिए कई तात्कालिक व दीर्घकालिक योजनाएं शामिल हैं, जो यकीनन देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी।
लेकिन राहत पहुंचाने के इन प्रयासों के बीच कृषि विशेषज्ञ कई बिंदुओं को लेकर आशंकित भी हैं। उनकी चिंता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन के बाद किसान कहीं और ज्यादा शोषण के शिकार न हो जाएं। प्रस्तावित अनाजों व तिलहन समेत अन्य कई उपज को मौजूदा कानूनी दायरे से बाहर किए जाने के बाद किसानों के पास फसलों को सिर्फ सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचने का विकल्प नहीं होगा। स्पष्ट है, सरकार मानकर चल रही है कि किसान निजी व्यापारियों को अपनी उपज बेचकर शायद ज्यादा लाभ कमा सकेंगे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब अनाज जमा करने को लेकर कोई रोक-टोक नहीं रहेगी और अकाल जैसी स्थितियों को छोड़ यह अधिनियम प्रभावी नहीं रहेगा। इस निर्देश के पीछे की मंशा किसानों के लिए कल्याणकारी है, पर इसके दूरगामी परिणाम कुछ और निकल सकते हैं। अबाध भंडारण के दीर्घकालिक रूप से प्रभावी होने पर दो बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पहली, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत मिलने की आशंका अधिक है। और दूसरी, निजी खरीदारों द्वारा भारी मात्रा में जमाखोरी से सरकारी खाद्य भंडारण व खाद्य सुरक्षा की मौजूदा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
भारत जैसे आर्थिक संरचना वाले देश में अनाज भंडारण पर सरकारी नियंत्रण बेहद आवश्यक है। कल्पना कीजिए, यदि आज की स्थिति में अनाज भंडारण निजी क्षेत्र व व्यक्ति विशेष के हाथों में होता, तो भूख से मरने वालों की तादाद कितनी होती? आज भारतीय खाद्य निगम के पास 524 लाख टन का खाद्यान्न भंडार है। यह मात्रा अकाल और भुखमरी से बचाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। पर यदि निजी हाथों में खाद्यान्न भंडारण देने का कानून बना, तो भविष्य में आपात स्थितियों में अनाज की आपूर्ति की स्थिति विषम हो सकती है। निस्संदेह, अनाज की उपलब्धता तो होगी, मगर शर्तें तब निजी घरानों की ही लागू होंगी। कई कृषि विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है कि निजी नियंत्रण के बाद मुनाफे के चक्कर में अधिकांश अनाज निर्यात भी किया जा सकता है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावित हो सकती है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में संसद ने इस मकसद से पारित किया था कि ‘आवश्यक वस्तुओं’ का उत्पादन, आपूर्ति व वितरण को नियंत्रित किया जा सके, ताकि ये चीजें उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर उपलब्ध हों। आवश्यक वस्तु की श्रेणी में घोषित वस्तुओं का अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने का अधिकार सरकार के पास होता है। तय मूल्य से अधिक कीमत लेने पर विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। मार्च में बढ़ते वायरस-संक्रमण के बीच मास्क व सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से सरकार को इन दोनों वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में डालना पड़ा था।
खरीफ व रबी फसलों के लिए प्रत्येक मौसम में एमएसपी की घोषणा की जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक राज्य से ऐसी शिकायतें आती रहती हैं कि किसानों को उनके उत्पाद का एमएसपी नहीं मिल रहा है। कृषि मंत्रालय और नीति आयोग, दोनों स्वीकार कर चुके हैं कि किसान घोषित एमएसपी से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में, नए कानून से जुड़ी अब तक की घोषणाओं से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि निजी खरीदारों के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मानना जरूरी होगा या नहीं? किसानों को लाभ तभी मिल पाएगा, जब निजी खरीदारों द्वारा दिए जाने वाले मूल्य की गारंटी सुनिश्चित होगी।
(ये लेखक के अपने विचार हैं