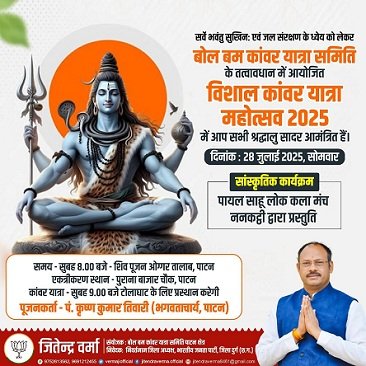सम्पादकीय / शौर्यपथ / यह सचमुच कडे़ इम्तिहान की घड़ी है। प्रकृति जैसे हमारे समूचे धैर्य और संघर्ष-शक्ति को आजमाने पर उतर आई है। एक तरफ, दुनिया कोविड-19 के कहर से हलकान है, तो वहीं दूसरी ओर चक्रवाती तूफान कई देशों के लिए विनाशकारी बनकर आया, और अब लू के थपेड़ों ने धरती के जीवों को झुलसाना शुरू कर दिया है। भारत के कुछ हिस्सों में तो पारा सोमवार को 47 डिग्री के पार चला गया और मौसम विभाग का आकलन है कि इस बार मानसून देरी से केरल पहुंच रहा है यानी सूरज देव का कोपभाजन लंबे समय तक बनना पडे़गा, खासकर उत्तर भारत के लोगों को। चढ़ते पारे के कारण मौसम विभाग ने कल दिल्ली में ‘ऑरेंज अलर्ट’ तक जारी किया था। ऐसी सूचनाएं लोगों को आगाह करती हैं कि वे बेवजह धूप में न निकलें।
जब कोरोना महामारी के कारण देश-दुनिया में पूर्ण लॉकडाउन हुआ, और कारों-कारखानों के पहिए थमे, तब पर्यावरण में कई तरह के सुखद बदलाव दर्ज किए गए थे। शहरों की हवा, नदी-जल के प्रदूषण में कमी के अलावा सुदूर आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्रों के भरने तक की खबरें आईं। लेकिन तब भी मौसम वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने किसी तात्कालिक राहत की उम्मीद नहीं बांधी थी, और अब जिस तरह से तापमान नए रिकॉर्ड दर्ज कराता जा रहा है, उसे देखते हुए शासन-प्रशासन के आगे एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि पिछले एक दशक में 6,000 से भी अधिक लोग लू के शिकार बन चुके हैं। और यह आंकड़ा सिर्फ उन लोगों का है, जिनके नाम सरकारी दस्तावेजों में इस खाते में दर्ज हुए। ऐसे में, शासन-प्रशासन के ऊपर अब दो-दो मोर्चों पर जूझने की जिम्मेदारी होगी। एक तरफ, उन्हें कोविड-19 के संक्रमितों के क्वारंटीन और इलाज की व्यवस्था करनी है, तो वहीं लू के लिहाज से बेहद संवेदनशील लोगों की मदद के लिए भी तत्पर रहना है। चिंता की बात बस यह है कि पिछले दो महीने से भी अधिक समय से अनिवार्य सेवाओं से जुडे़ लोग अनथक अपने कर्तव्य के निर्वाह में जुटे हुए हैं, तापमान के इस तीखे तेवर से उन पर काम का बोझ और बढ़ जाएगा।
देश के कई महानगर पहले ही भारी जल संकट झेल रहे हैं। खासकर गरमी के तीन-चार महीनों में तो उनकी हालत सबसे दयनीय होती है। पिछले साल मुंबई, बेंगलुरु में पानी की किल्लत का आलम यह रहा कि कई बडे़ आयोजन तक टाल देने पडे़ थे। आज जब मुंबई और चेन्नई जैसे महानगर कोरोना महामारी से सर्वाधिक त्रस्त हैं, तब किसी प्रकार का जल संकट उनके लिए परेशानी का एक नया सबब बन सकता है। लोगों की दैनिक जरूरतों के लिए पानी की कमी होगी, जबकि बेहतर सैनेटाइजेशन के लिए उन्हें अधिक पानी की जरूरत होगी। यह ठीक है कि बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय कामगारों के वहां से पलायन के कारण नगर प्रशासन का दबाव कुछ घटा होगा, लेकिन विडंबना यह है कि हमारे नागरिक जीवन की जितनी जमीनी सेवाएं हैं, उनका दारोमदार काफी कुछ बाहर से आए मजदूरों के कंधों पर ही रहा है। इसके लिए किसी बड़े समाजशास्त्रीय अध्ययन की जरूरत भी नहीं। एक बात और। न तो कोरोना शहर-गांव, अमीर-गरीब में कोई फर्क कर रह रहा है और न ही लू के थपेडे़ करेंगे, इसलिए यहां भी एहतियात ही इलाज है।